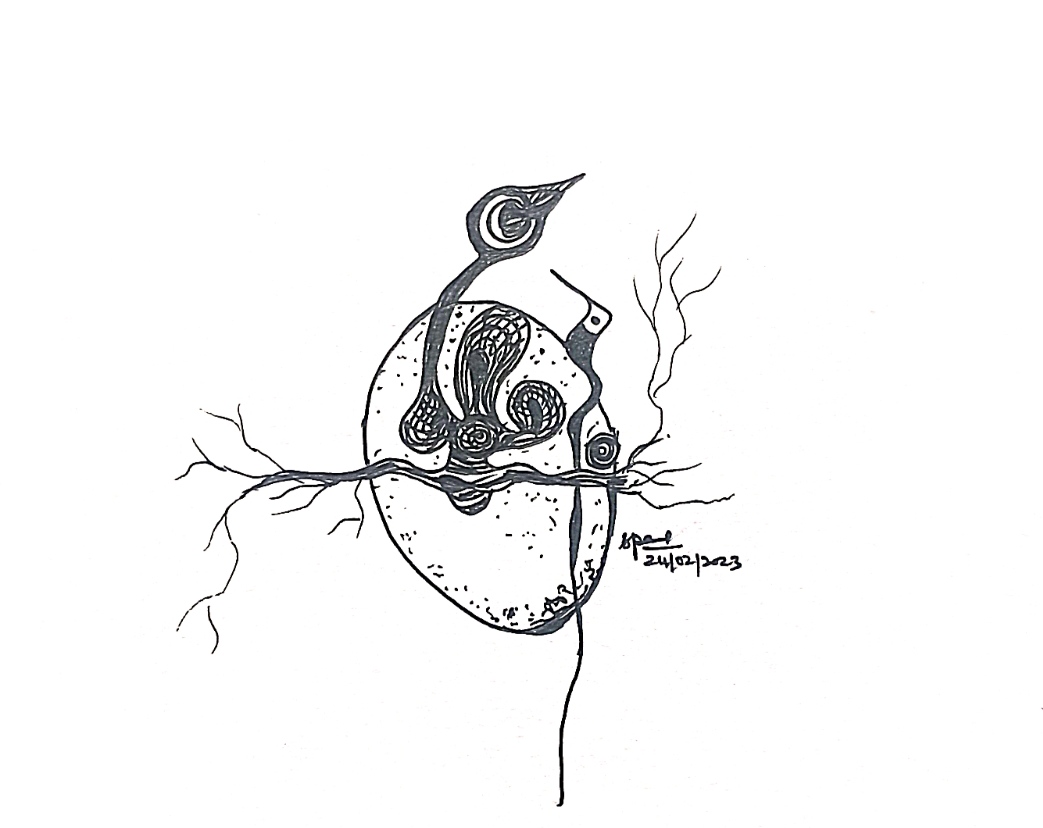
समकालीन कविता

इसाबेला फिलिपिएक Izabela Filipiak
Karen Kovacik के अंग्रेजी अनुवाद से हिन्दी में रति सक्सेना द्वारा अनूदित
घरेलू मिथक
मेरी जिनी रसोई में काम करती है
मेरा टाइटनेस मुझे गर्म खाना खिलाती है
सुनिश्चित करती है कि मैं भूखा न रहूं
बर्तनों को उछालती है, एश ट्रे को साफ करती है
वह मुझसे कहती है: तुम बहुत दुबली-पतली चूजे हुआ करती थी
और अब तुम मेरे स्वादिष्ट छोटी मुर्गी में बदल गई हो
वह मुझे बिस्तर पर ले जाकर नदी में धुली चादर पर
सफ़ेद मूर्ति की तरह लिटा देती है
अभी भी एक ऑक्टोपस में लिपटा नमक से चमक रहा है
उसका आलिंगन उग्र से कुछ कम कोमल है
सीप की तरह सिकुड़ी हुई, मैंने खुद को भस्म होने दिया
पृष्ठभूमि में कहीं, वह मेरे स्नान के लिए पानी चला रही है
Karen Kovacik के अंग्रेजी अनुवाद से हिन्दी में रति सक्सेना द्वारा अनूदित
मैडम सहजज्ञानी
मेरा पूरा जीवन दूसरी भाषा सीखने जैसा है-
इतने सारे अप्रवासी बलिदान के बावजूद
इस उच्चारण से छुटकारा नहीं मिल पाता है,
हर जगह पहचान लिया जाता है यह, मैं निराश हूं
काफी कुछ जानलेने के बावजूद
सारा प्रयास निरर्थक, और किसलिए?
स्वीकार नहीं कर पाने से हतोत्साहित हूं,
मैं बातचीत सिखाने वाली क्लास में दाखिला लेती हूं
वहां मैं भी वही पुराने लहजे में बोलती हूं
कभी कभी सारे सूत्र कनेक्शन टूट जातेहैं
मैं सोचती हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती
आप इसे ‘मातृभाषा’ कह सकते हैं
लेकिन मेरी माँ नहीं है, केवल कुछ
पुराने किस्से और मिथक: लोग देख कर विचलित होते हैं
रस्सी पर नाचती महिला को-क्या वह गिर जाएगी?
क्या उसे पकड़ने के लिए कुछ मिलेगा?
उसके मूड में बदलाव का ध्यान से रेखांकन
उच्चारण में शुद्धता नहीं देता
वह दूसरी भाषा, मायावी फिर भी परिचित, पानी की तरह है:
मेरी उंगलियों से फिसल जाती है, अब फिर से खाली हो गया है
लेकिन नमी के एक अंश के बाद फिर से रिक्त, एक बाद का स्वाद
क्रिस्टलीय आनंद के बाद का स्वाद, प्रारंभिक पुनर्जागरण कवि की तरह,
मैं तर्क और संक्षिप्तता के साथ
लैटिन की विस्तृत अंडरगर्डिंग का स्वाद लेती हूं
विस्तृत अध्ययन के बावजूद
यह कभी भी पूरी तरह से कभी गायब नहीं होगा.
शिक्षित वर्ग की भाषा
मुझे अलंकारिक प्रतियोगिताओं में बढ़त मिलती है।
लेकिन बहस करते वक्त मैं
नियमों को भूल जाती हूं,
शब्दों की उत्पत्ति अनिश्चित हो जाती है।
अपने बारे में अनिश्चित होकर, मैं बोलना बिल्कुल बंद कर देती हूं
और बस ध्वनियों के प्रपात को सुनती हूं
चट्टानों की घाटी पर गिरती हुई एक पहाड़ी जलधारा
जो एक अस्थिर नाड़ी, एक प्रतिध्वनि की तरह गायब हो जाती है,
अब तुम मुझे सुनते हो, अब नहीं-
और इससे पहले कि मैं हंस सकूं, मुझे आगे बढ़ना होगा
चोट और शर्म का सामना कैसे करें?
अन्यत्र मुझे पत्रों के टुकड़े, टूटी हुई कहानियां मिलती हैं।
मैं उन ढीले सिरों को बांधती हूं, अपने ब्रश से रेखाओं को पुनर्स्थापित करती हूं।
मैं संतुष्ट हूं, मैं केवल देखती हूं, मैं कुछ नहीं कहती,
सांस लेने की हिम्मत भी नहीं ताकि डर न लगे
यह सड़क किनारे का प्राणी आधी औरत, आधा जानवर।
जब मैं पलट कर दोबारा उस तरफ देखती हूं
तो क्या मुझे उसके छोटे खुर से कम से कम एक प्रिंट मिलेगा?
Karen Kovacik के अंग्रेजी अनुवाद से हिनदी में रति सक्सेना द्वारा अनूदित
इसाबेला फिलिपिएक पोलिश साहित्य की समकालीन महत्वपूर्ण लेखिका हैं, कहानियां, निबन्ध के अतिरिक्त कविताएं भी रची हैं। वे पोलिश साहित्य में नव लेखन की प्रतिनिधि हैं। 

इसाबेला फिलिपिएक पोलिश साहित्य की समकालीन महत्वपूर्ण लेखिका हैं, कहानियां, निबन्ध के अतिरिक्त कविताएं भी रची हैं। वे पोलिश साहित्य में नव लेखन की प्रतिनिधि हैं।इनका जन्म 1962 में पोलैंड में हुआ लेकिन वर्तमान में सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं। ये दस पुस्तकों की लेखिका हैं, उन्होंने काफी आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की है, और उनके लेखन का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने अपनी मातृभूमि के साथ साहित्यिक और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए, अमेरिका में भी स्वयं को स्थापित किया है, उन्होंने कैलिफोर्निया के कॉमनवेल्थ क्लब में पोलिश समलैंगिक/लेस्बियन/उभयलिंगी/ट्रांसजेंडर और महिलाओं के अधिकारों पर भाषण दिए और बीट्राइस एम. बैन रिसर्च ग्रुप में भाग लिया।
गौरव सिंह
आत्मस्वीकार-1
जो अपराध मैंने किये,
वो जीवन जीने की न्यूनतम ज़रूरत की तरह लगे !
मैंने चोर निगाहों से स्त्रियों के वक्ष देखे
और कई बार एक लड़की का हृदय ना समझ सकने की शर्म के साथ सोया..
मुझे परिजनों की मौत पर रुलाई नहीं फूटी
और कई दफ़े चिड़ियों की चोट पर फफककर रोया..
मैं अपने लोगों के बीच एक लम्बी ऊब के साथ रहा
और चाय बेचती एक औरत का सारा दुःख जान लेना चाहा…
मैंने रातभर जागकर लड़कियों के दुःख सुने
पर अपनी यातनाएं कहने के लिए कोई नदी खोजता रहा
मुझे अपनी पीड़ाएं बताने में संकोच होता है
मैं बीमारी से नहीं, उसकी अव्याख्येयता के कारण कुढ़ता हूं …
जीवन के कई ज़रूरी क्षण भूल रहा हूं
और तुम्हारे तिलों की ठीक जगह ना बता पाने पर शर्मिंदा हूं…
मुझ पर स्मृतिहीन होने के लांछन ना लगाओ
मैं पानी के चहबच्चों की स्मृतियाँ लिए शहर-दर-शहर भटक रहा हूं
जितनी मनुष्यता मुझे धर्मग्रंथों ने नहीं सिखायी
उससे कहीं ज़्यादा प्रेम एक बीस साल की लड़की ने सिखाया
प्रेम में होकर मैंने ज़िन्दगी पर सबसे अधिक गौर किया
मैं यह मानने को तैयार नहीं कि प्रेम किसी को जीवन से विमुख कर सकता है…
आत्मस्वीकार-2
बहुत कम फूलों के नाम जानता हूं
तितलियों की कम प्रजातियां देखी हैं जीवन में
हिंस्र पशुओं को सिर्फ चिड़ियाघर के बाड़ों में कैद देखा है
कविता के बिम्ब की तरह कुमुदिनी लिखते हुए कई बार हाथ कांपे हैं…
सैकड़ों ज़रूरी बातें
निरर्थक प्रलाप की तरह कानों से गुजर जाती हैं
सालों पहले देखे एक झरने की स्मृति से देह सिहरती है…
प्रेम के निविड़तम क्षणों में
नौकरी की प्रस्तावित तिथियों के बारे में सोचता हूं
और नदियों को देखकर अबतक अपने खानाबदोश न बन पाने को कोसता हूं…
तानाशाहों से बचने को
कविता का सबसे कीमती टुकड़ा बुहार देता हूं
पर किसी की ख़ुशी के लिये कविता में एक पंक्ति भी नहीं लिखता..
असहमतियों के कारण असुरक्षित हूं
और कभी अपनी जीवटता पर मुग्ध भी
कि मैंने असाध्य कांपती उंगलियों से कविताएं लिखी हैं…
चांद एक दुर्घटना की तरह याद रहता है
दिल में विक्षत कविताओं के अनगिन टुकड़े हैं
तुम्हारी सांत्वनाएं मेरे लिये निरर्थक हैं…
स्त्रियां
उनकी आत्मा पर कई ऐसे निशान हैं
जिनके बारे में इतिहास कुछ नहीं कहता
और कुछ पूछने पर
धर्मग्रन्थ भी चुप्पी साध लेते हैं…
उनकी हँसी में
दुःख इस तरह घुल गये हैं
कि हँसने और रोने के
बीच का सारा भेद मिट गया है
कभी वे हँसते-हँसते रो देती हैं
तो कभी रोते हुए हँस पड़ती हैं…
उनकी देहें
सभ्यताओं के इतिहास-लेखन का
सबसे प्राथमिक स्रोत हो सकती थीं…
अगर कवियों ने उसका इत्र बनाकर
बूढ़े और लम्पट राजाओं को न बेचा होता..!
उनको मनाने के लिए
भाषा के पास सबसे संयत ध्वनियां हैं
और चुप कराने के लिए
भाषाओं ने सबसे विकृत गालियां ईजाद कीं…
अपनी घृणित वासना पर
उत्प्रेक्षाओं की सजावट लगाकर
वे उनके रूप और सुकोमल देह की ऐसी प्रशंसा करते
कि सैकड़ों बूढ़ी, लोलुप आंखें कामातुर हो उठतीं…
शताब्दियों तक
उनके कुचाग्र, नितम्ब
और उरोजों के लिए उपमाओं से लदी कविता
इन स्त्रियों के हृदय के बारे में कुछ नहीं जानती
और उनके उरोज भी श्रीफल की तरह बिल्कुल नहीं हैं…
गौरव सिंह

गांव – ईश्वरपुर साई, मल्लावां ज़िला- हरदोई, उत्तर प्रदेश में जन्में युवा कवि गौरव सिंह ने
स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू महाविद्यालय तथा परास्नातक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। वर्तमान में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं।
अनुपमा तिवाड़ी
1. स्त्री का चित्र
ट्रकों के पीछे ‘तुम कब आओगे’
की मुद्रा में प्रतीक्षारत औरत तुम्हें
अच्छी लगती है न !
डोरमैट और पोस्टर्स पर स्त्री के जुड़े हाथ
स्वागत की मुद्रा में तुम्हें
अच्छे लगते हैं न !
स्त्री के गालों पर लुढ़कते आंसू के चित्र तुम्हें
अच्छे लगते हैं न !
एक डरती,
दबती,
आजिजी करती स्त्री तुम्हें
अच्छी लगती है न !
मुझे अच्छी नहीं लगतीं।
मुझे आसमान तकती स्त्रियां पसंद हैं।
आसमान तकती स्त्री का चित्र बनाने के लिए
पहले चित्रकार को आसमान ताकना होता है।
2. पानी – पानी
दुनिया का सबसे महंगा पानी पीती हैं
आधुनिक रानी।
उनकी 750 मिलीलीटर की एक बोतल की कीमत 40 लाख रुपए के करीब है।
मेरी हँसी और रुलाई मिक्स हो जाती है यह पढ़कर
और आंखों में ‘ठाकुर का कुआ’ की तथाकथित दलित स्त्री आ जाती है
जो अपने बीमार पति के लिए अपनी जान और इज्ज़त दांव पर लगाकर
ठाकुर के कुए से पानी चुराती है।
मेरी आंखों में आ जाते हैं
ऐसी तमाम स्त्रियों के चित्र
जो तीन – तीन मील दूर से चिलचिलाती धूप में मटके – पे – मटका माथे पे रखकर लाती हैं पानी।
कल दूर के एक गांव में लड़ मरी थीं दो स्त्रियां पानी की बारी पर।
मेरी आंखों में आ जाते हैं वो चित्र
जिसमें किसी बड़े कुए में ढेर सारी रस्सियां लटकी हैं
और पानी निकालने की जुगत में झुके हैं तमाम सिर।
मेरे सामने आ जाती हैं अखबार की वो कटिंग
जिसमें हैण्डपम्प पर चरियां, मटके, डोलची और बाल्टियां बैठे हैं,
एक लम्बी कतार में।
मेरी आंखों के सामने आ जाती है
ये इबारत कि
सावित्रीबाई फुले ने प्यासे मरते तथाकथित दलितों के लिए कुआ खुदवा दिया था।
मेरे ज़ेहन में आते हैं ऊंट
जो एकसाथ कई दिनों का पानी पी कर
इंतजाम कर लेते हैं अपना।
मैं देखती हूं अब कितनी ही प्याऊओं का पानी घुस गया है बोतलों में।
मैंने सुना और देखा है कि अब होटलों में पौना गिलास पानी दिया जाता है।
यूं पानी की कहानी कहते – कहते
मेरी आंखों में आ जाता है पानी।
अब मैंने रानी के पानी की कीमत तो जान ली
अब मैं उनके पेशाब की कीमत जानना चाहती हूं।
3. भूख
बिना हथियार के भी
मर सकता है
गरीब और मजबूर आदमी।
उसका रोज़गार छीन लो,
धकिया दो उसे,
छोड़ दो सड़कों पर उसे बेसहारा,
आखिर,
कहां जाएगा ?
कैसे जीएगा ?
खुद ही आत्महत्या कर लेगा।
साफ़ – सुथरी तमाम तफ्तीशें और
पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेंगी
कुछ नहीं निकला।
चलो,
हम सब मुक्त हुए !
आखिर,
वो बहुत काम का भी क्या था ?
अनुपमा तिवाड़ी– राजस्थान जयपुर की कहानीकार,  शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता और कवयित्री अनुपमा तिवाड़ी के तीन कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह ,एक शिक्षा पर पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। आपके देश – विदेश की 125 से अधिक पत्र – पत्रिकाओं में रचनाएं व लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता और कवयित्री अनुपमा तिवाड़ी के तीन कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह ,एक शिक्षा पर पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। आपके देश – विदेश की 125 से अधिक पत्र – पत्रिकाओं में रचनाएं व लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
 शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता और कवयित्री अनुपमा तिवाड़ी के तीन कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह ,एक शिक्षा पर पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। आपके देश – विदेश की 125 से अधिक पत्र – पत्रिकाओं में रचनाएं व लेख प्रकाशित हो चुके हैं।
शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता और कवयित्री अनुपमा तिवाड़ी के तीन कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह ,एक शिक्षा पर पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। आपके देश – विदेश की 125 से अधिक पत्र – पत्रिकाओं में रचनाएं व लेख प्रकाशित हो चुके हैं।आलोक रंजन
चिन्ताएं
मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठकर
पढ़ रहा था,
सबके चेहरे।
सबके चेहरे पर
लिखी हुई थीं चिन्ताएं।
मैं तलाश में था,
मिल जाए कोई
ख़ुश चेहरा।
ताकि देखकर
मैं भी हो जाऊं ख़ुश।
आख़िरकार
असफल रहा मैं।
आज के भी दौर में,
जहां मनोरंजन के लिए बनते हैं
रोज़ नए यूट्यूब चैनल।
अच्छा लगता है
जब औरतें बोलती हैं
विरोध के स्वर
तो अच्छा लगता है।
और अच्छा लगता है,
जब वह घर परिवार और
रिश्ते-नाते छोड़ अपने-अपने
कर्तव्यों और अधिकारों की करती हैं बातें।
बहुत अच्छा लगता है,
जब वह नेताओं पर गालियां
फेंककर मारती हैं तमाचा।
मांगती हैं वह अपने
वोटों का हिसाब,
खोजती हैं फ़ाइलें काम की।
अंतिम दरवाज़ा
जब पापा देर से घर आते हैं
देर से बंद होता है
अंतिम दरवाज़ा!
हम कर रहे होते हैं
दुनिया का सबसे बड़ा इन्तज़ार।
हम मिलाते रहते हैं फ़ोन
आख़िरी वक़्त तक,
करते रहते हैं उनकी बात
वह उपस्थित होते हैं,
हमारी बातों में।
कभी कभार तो
बहुत देर से आ पाते हैं।
साग-सब्ज़ी, तेल-साबुन, नून-मसाला….
लेकिन देर नहीं होती
आवश्यकताएं पूरी होने में।
चेक होने लगती हैं
उनकी डिग्गी,
हेल्मेट में जो ख़ाली जगह
कोई तो सामान
मिल जाए खाने के लिए।
मुझे मरना है
मुझे अब मरना है
लेकिन आत्महत्या करके नहीं,
किसी दुर्घटना की चपेट में।
क्योंकि बच्चे मर रहे मेरे
तड़प तड़प कर,
कुछ नहीं उनके पेट में।
हां, ग़लती थी हमारी,
है भी हमारी
और रहेगी भी।
क्यों नहीं कुछ रहना भी
तो चाहिए प्लेट में।
ग़रीबी से तो सही
हम जात से भी लड़ते हैं,
यूं ही नहीं वे रगड़ते हैं
नाक स्लेट में।
हँस मत, पागल सब क्या सोचेंगे,
जब तू ही पढ़ लेगा फिर किसे नोचेंगे
होटल में बिक गया आज वो भी मेरे रेट में।
आलोक रंजन कवि गीतकार, साहित्यकार,कैमूर, बिहार

मोबाइल- 9155113056

