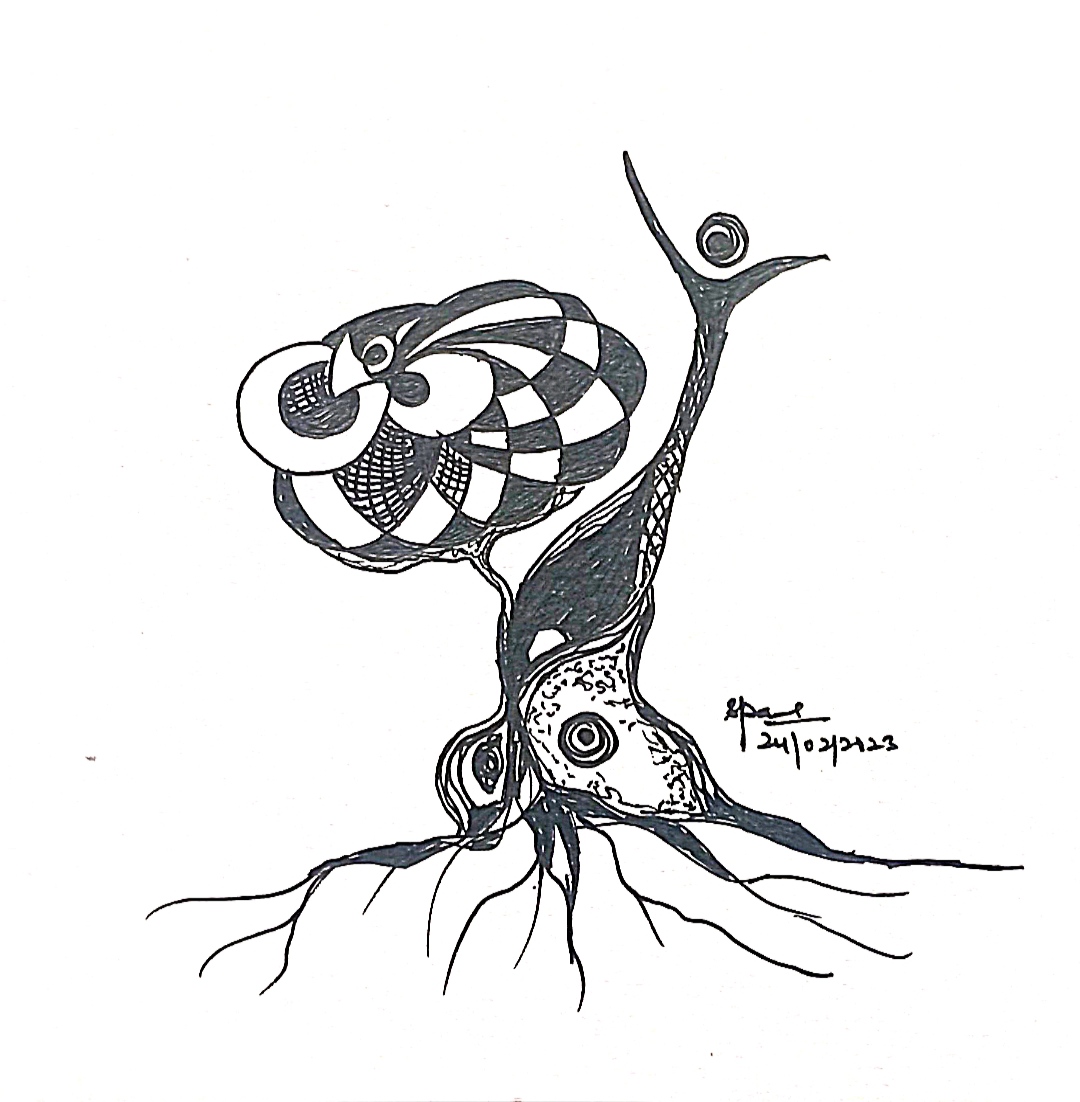
प्रिय कवि

हरि राम मीणा
1. सबसे छोटी कविता 
जो ज़मीन से नहीं जुड़े, वे ही जमीनों को ले उड़े!
2. मज़दूर
पसीना पोंछते-पोछते उसने तेज कर दी / अस्थमेटिक फुफ्फुस-सी धौंकनी को
ऊँघती भट्टी चेती, तेवर कुछ तल्ख हुए
संडासी के जबड़े में भिंचा लोहा पसीजने लगा
लुहारिन के हाथों में थमे घन की ताबड़तोड़ चोटें…..
और वह सख्त लोहा / अब गुंदी मिट्टी के लोथड़ा-सा
तब्दील होने लगा हल के पैने फाल में।
3. किसान
जेठ की लू उगलती दुपहरियों में
वह तराशता रहा बंजड़ जमीन को
पसीने से माटी कुछ गीली हुई
जैसे ही उम्मीद भरा आखिरी फावड़ा मारा
जमीन खिसक गई उसकी गिरफ्त से।
अब की बार वह फावड़े को सतौले हुए था
आँखों के काले हीरे को लक्ष्य पर टिकाते हुए।
4. आदिवासी लड़की
आदिवासी युवती पर वो तुम्हारी चर्चित कविता
क्या खूबसूरत पंक्तियाँ हैं- ‘गोल-गोल गाल, उन्नत उरोज, गहरी नाभि
पुष्ट जंघाएँ, मदमाता यौवन …….’
यह भी तो कि- ‘नायिका कविता की स्वयं में सम्पूर्ण कविता
ज्यों हुआ साकार तन में प्रकृति का सौन्दर्य सारा
रूप से मधु झर रहा एवं सुगन्धित पवन उससे ……’
अहा, क्या कहना कवि तुम्हारे सौन्दर्य-बोध का.
अब इन परिकल्पित-ऊँचाइयों पर / स्वप्निल भाव-तरंगों के साथ उड़ते
कलात्मक शब्द-यान से नीचे उतर कर
चलो उस अंचल में / जहाँ रहती है वह आदिवासी लड़की
देखो गौर से उस लड़की को
जिसके गोल-गोल गालों के ऊपर ललाट है
जिसके पीछे दिमाग / दिमाग की कोशिकाओं पर टेढी-मेढ़ी खरोंचें
यह एक लिपि है
पहचानो, इसकी भाषा और इसके अर्थ को.
जिन्हें तुम उन्नत उरोज कहते हो
प्यारा-सा दिल है उनकी जड़ों के बीच / कँटीली झाड़ियों में फँसा हुआ
घिरा है थूहर के कुँजों से / चारों ओर पसरा विकट जंगल
जंगल में हिंसक जानवर / जहरीले साँप-गोहरे-बिच्छू
इस केनवास में उस लड़की की तस्वीर बनाओ कवि.
अपना रंगीन चश्मा उतार कर देखो
लड़की की गहरी नाभि के भीतर / पेट में भूख से सिकुड़ी उसकी आँतों को
सुनो उन आँतों का आर्तनाद
और अभिव्यक्त करने के लिए / तलाशो कुछ शब्द अपनी भाषा में.
उतरो कवि, लड़की की ‘पुष्ट’ जंघाओं के नीचे / देखो पैरों के तलुओं को
विबाइयों भरी खाल पर / छाले-फफोलों से रिसते स्राव को देखो
कैसा काव्य-बिम्ब बनता है कवि.
और भी बहुत कुछ है. उस लड़की की देह में
जैसे- हथेलियों पर उभरी / आटण से बिगड़ी उसकी दुर्भाग्य-रेखाएँ
सारे बदन से चूते पसीने की गन्ध
यूँ तो चेहरा ही बहुत कह देता है और आँखों के दर्पण में
उसके कठोर जीवन का प्रतिबिम्ब है ही.
बन्द कमरे की कृत्रिम रोशनी से परे / बाहर फैली कड़ी धूप में बैठकर
फिर से लिखना / उस आदिवासी लड़की पर कविता.
5. बिरसा मुंडा की याद में
अभी-अभी सुन्न हुई उसकी देह से / बिजली की लपलपाती कौंध निकली
जेल की दीवार लाँघती / तीर की तरह जंगलों में पहुँची
एक-एक दरख्त, बेल, झुरमुट, पहाड़, नदी, झरना
वन प्राणी-पखेरू, कीट, सरीसृप
खेत-खलिहान, बस्ती, वहाँ की हवा, धूल, जमीन में समा गई ………………
एक अनहद नाद गूँजा – ‘मैं केवल देह नहीं / मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ
पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं / मैं भी मर नहीं सकता
मुझे कोई भी / जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता
उलगुलान! उलगुलान!! उलगुलान!!!
जंगल की धरती की बायीं भुजा फड़की
हरे पत्तों में सरसराहट / सूखों में खड़खड़ाहट
फिर मौन हो गया / कुछ देर के लिए सारा अंचल।
खेलने-कूदने की उम्र में / लोगों का आबा (भगवान) बन गया था वह
दिकुओं के खिलाफ / बाँस की तरह फूटा था धरती से
जैसे उसी पल गरजा हो आकाश / और काँपे हों सिंहों के अयाल।
नौ जून, सन् उन्नीस सौ / सुबह नौ बजे
राँची की वह आतताई जेल / जल्लादों का बर्बर खेल
अंतत: बिरसा की शान्त देह!
‘क्या किया जाए इसका?’
हैरान थे दिकुओं (बाहरी शोषक) के ताकतवर नुमाइंदे
जिन्दा रहा खतरनाक बनकर
मार दिया तो और भी भयानक
अगर दफनाया तो धरती हिलेगी / जो जलाया-आँधी चलेगी।
वह मुंडारी पहाड़ों-सी काली काया
नसें, जैसे नीले पानी से लबालब खामोश नदियाँ
उभरे पठार-सी चौड़ी छाती
पथराई आँखें- जैसे अभी-अभी दहकते अंगारों पर
भारी हिमखण्ड रख दिए हों।
कुछ देर पहले ही तो हुई थी खून की कै
जेल कोठारी के मनहूस फ़र्श पर
उसी के ताजा थक्के …..
नहीं! थक्के न कहें,
वे लग रहे थे- हाल ही कुचले पलाश के फूल
या खौलते लावा की थोड़ी-सी बानगी।
चेहरे पर मुरझाई खाल की सलवटों की जगह
उभर आया एक खिंचाव
जैसे, रेशा रेशा मोर्चाबन्द हो गिलोल की मानिन्द
धनुष की कमान-सी तनी माँसपेशियाँ
रोम-रोम जैसे- तरकस में सुरक्षित असंख्य तीरों की नोंक
गोया, वह निस्पन्द बिरसा न होकर
आजाद होने के लिए कसमसाता समूचा जंगल हो।
उन्हें इन्तजार था सूरज के डूब जाने का
दिनभर के उजास को वे छुपाते रहे सुनसान अंधी गुफा में
जिसके दूसरे छोर पर गहरी खाई
वहीं उन्होंने बिरसा मुंडा से निजात पाई।
कहते हैं- काले साँप को मारकर गाड़ देने से
खत्म नहीं हो जाती यह सम्भावना कि / पुरवाई चले और वह जी उठे
यदि ऐसा हो तो
परिपक्व जीवन को धरती अपने गर्भ में नहीं रखती।
बिरसा उनके लिए साँप से खतरनाक था
वह दिकूभक्षी शेर था और वह भी अभी जवान।
इसलिए उसे दफनाया नहीं / जलाया था रात के लिहाफ में छुपाकर
यह जानते हुए भी कि दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं
जो दूसरी आग को जलाकर राख कर दे।
रात के बोझिल सन्नाटे ने स्वयं को कोसा
आकाश के सजग पहरेदारों की आँखें सुर्ख हुईं
हवा ने दौड़कर मुंडारी अंचल को हिम्मत बँधाई
उन्होंने आदमी समझकर बिरसा को मार दिया
मगर बिरसा आदमी से बढ़कर था
वह आबा, वह ‘भगवान्’ / वह जंगल का दावेदार
उसकी आवाज जंगलों में अभी भी गूँजती है-
‘मैं केवल देह नहीं / मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ
पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं / मैं भी मर नहीं सकता
मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता
उलगुलान! उलगुलान!! उलगुलान!!!
6. विक्षिप्त राष्ट्र
स्वप्नलोक की अर्द्धरात्रि के अवचेतन में
दिखा मुझे-
उलझे केशों को खींच रहा विक्षिप्त राष्ट्र
दोनों हाथों के लम्बे तीखे नाखूनों से
ज्यों घने जूट के जंगल में / हल जोत रहा कोई किसान
बंजड़ धरती की छाती में हल-फाल जा रहा धँसा
उधर शीश की त्वचा हो रही रक्तस्नात
परिवर्तित होती रिक्त पटल में
जिस पर दृश्यों का क्रम अंकित हो रहा स्वत:
वह चित्रमयी लिपि, अपठ पहेली को सुलझाते
टूट गया मेरा प्रयत्न-क्रम
छूट गया वह स्वप्न नींद की डोरी से
अब मेरा चेतन खोज रहा अवचेतन के उन दृश्यों को
जो नहीं तिरोहित
हैं मानस की स्मृति के खण्डों में अवरोहित
जो मुझे सिखाया गुरुओं ने जिन ग्रंथों से-
‘सत्यम ब्रूयात, सत्यमेव जयते, बहुजन हिताय:
तम सो मा ज्योतिर्गमय’
-क्या वह भ्रम था
अथवा
इन सूत्रों के अब अर्थ हो गए परिवर्तित
‘ओ मेरे प्रिय राष्ट्र, बताओ!
तुझको कंधों पर लादे
हाथों में तेरा ध्वज थामे
ये शंखनाद करते नायक
उद्घोषों से प्रज्जवलित अग्नि
सिंदूरी होता नील गगन / काँपती धरा
यह दृश्य देख
मैं मकड़जाल की भूलभुलैया में भटका
ज्यों अष्टभुजाधारी की जकड़न में अटका
जैसे मेरे वे स्वप्न हो गए गड्डमड्ड
पहले से उलझा हूँ जिनको सुलझाने में
चेतना हो रही है बेसुध
हो रहा भयंकर तेरे विराट जन का दोहन
समृद्ध धरा-धन का दोहन
फिर भी दोहक के प्रति यह कैसा सम्मोहन
जिससे विगलित होती जाती तेरी गरिमा
मैं विचलित हूँ
आँखों के आगे अँधेरा
तुझको, मुझको
आखिर किस भय ने हमको आ घेरा
तुम अवचेतन में मुझे दिखे थे-
खींच रहे दोनों हाथों से अपने उलझे केशों को
मैं भींच रहा मस्तिष्क ग्रन्थियों को भीतर
जिनकी सब रक्त-वाहिकाओं में यह नीला जल
दौड़ता जा रहा तोड़-ताड़ सारे बंधन
यह रुधिरहीन सम्पूर्ण देह
पीली-पीली, नीली-नीली, काली-काली
बस आँखों में है लाल लहू अथवा लावा
फूटता नहीं, बह रहा नहीं,
उससे कोई भी तो जल रहा नहीं
क्यों है सुसुप्त, अनभिव्यक्त अभी?
-मैं पूछ रहा खुद से
जूझ रहा खुद से!
हरिराम मीणा आदिवासी समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी, कवि, चिंतक, विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कविताओं में प्रस्तुत उनकी वैचारिकी समस्त आदिवासी समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में उनकी रचनात्मक सक्रियता आदिवासी यथार्थ की अभिव्यक्ति से आगे बढ़ते हुए समग्र मनुष्यता के सांद्र विश्लेषण तक विस्तृत हो जाती है।
उनके अब तक तीन कविता-संग्रह (‘हाँ, चाँद मेरा है’, ‘सुबह के इंतज़ार में’, ‘आदिवासी जलियाँवाला एवं अन्य कविताएँ’), एक प्रबंध-काव्य (‘रोया नहीं था यक्ष’), तीन यात्रा-वृतांत, एक उपन्यास, आदिवासी विमर्श की दो पुस्तकें तथा समकालीन आदिवासी कविता (संपादन) पर एक पुस्तक प्रकाशित हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से रचनाओं और वार्ता आदि का प्रकाशन एवं प्रसारण हुआ। उनकी पुस्तकें देश के दर्जनों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। उनके साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के सौ से ऊपर एम.फिल. एवं आधा दर्ज़न पीएच.डी. की जा चुकी है।
वह भारतीय पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक, वन्यजीव संरक्षण के लिए पद्मश्री सांखला अवार्ड, डा। अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च ‘मीरां पुरस्कार, केन्द्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान, बिड़ला फ़ाउंडेशन के बिहारी पुरस्कार और विश्व हिंदी सम्मान से विभूषित हैं।

