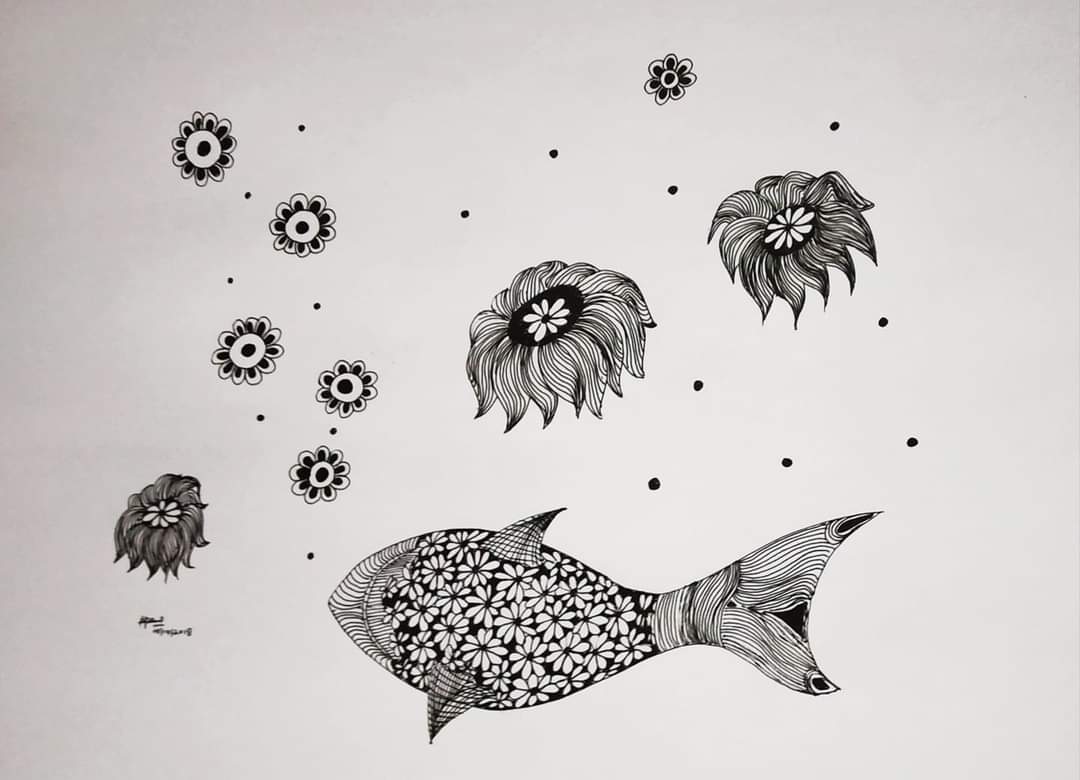
समकालीन कविता

आदित्य शुक्ला

फ़ासला
फासले से छुओ ताकि भरभराकर गिर न जाए
अगली पंक्ति
दूर तक बिखर न जाए
थोड़ी दूर तक चलने वाला अकेलापन
अनकहे लफ़्ज़
बहुत ख़ामोशी में पगी बेचैनी को थोड़ी देर और जलने दो सीने में
थोड़ी देर और ज़िंदगी की लौ भड़कने दो
जैसे आवारगी के दिनों में बेज़ार
पुराने साइकिलों पर भटकते थे
ढूंढते थे अर्थ फ़ाख़्ताओं की उड़ान में
कुछ फ़ासले पर रखो एक अर्थ
ताकि सिर टिकाने से वह सरककर दूर ना चला जाए
उन पुलों पर
जिनके नीचे से धड़कती गुज़रती है जीवन नदी
नदी जिसकी हर लहर के साथ दृष्टि दोनों क्षितिज माप ले
थाह ले
ख़याल
गुज़रे किनारों को
किनारे जो छूट गए
छूट गईं तन्हा रातें नींद की बेचैनी में
आंखों में चुभता अंधेरा
कभी शीतल, कभी तीखा;
पुल से गुजरने की ज़रूरत थी
धड़ धड़ाती रेल
अब गिरा कि तब गिरा की बेचैनी
इतना ही फासला
भय, यात्रा और सुकून में
सब कुछ एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर
इंतज़ार बना रहा।
कमी
बहुत कम थी कविताएं
और ज़रा सी थी सुंदरता
बहुत अधिक थी इच्छाएं और उनके ध्वंसावशेष
बहुत अधिक थी जल्दबाजियां
बहुत कम जगहें थी ठहरने की
अधिकताओं में भटकते हुए बहुत अधिक लोग थे
इतने अधिक कि उन्हें लिखने पर वाक्यों की सूरत बिगड़ जाती
पृथ्वी नाराज़गी में मुंह मोड़ लेती
और कमियां थीं हर ओर
हर चीज़ की, हर बात की
रोते बिलखते लोग थे हर ओर
पराजित हताश सभ्यता थी
स्मृतियों में भूलना था और वाक्यों में कुछ नहीं कहना..
नदी में जाल
नदी में जाल डालता हूं
एक भी नीली मछली नहीं आती है जिसमें
नदी में जाल डालने की क्रिया किसी स्मृति की तरह स्तब्ध रह जाती है
गांव के बच्चों का कोलाहल लिए
मैं जानबूझकर गिरा देता हूं अपनी कुल्हाड़ी नदी में
नदी देवी के अस्तित्व को सच मानकर
हक्का-बक्का होकर ताकने लगता हूं
लहरों की गतिविधियों को।
नदी मेरे मनोलोक में लोककथा की तरह बसती है।
मैं नदी में जाल डालकर छोड़ देता हूं
मैं नदी में कुल्हाड़ी फेंक देता हूं
भूल जाता हूं जाल, भूल जाता हूं कुल्हाड़ी
और लोग भी जाल डालते होंगे
और लोग भी कुल्हाड़ियां डालते होंगे
मैं कंकड़ फेंकता हूं तो नदी वापसी में पानी की छींटे देती है
नदी किनारे-किनारे चलता हूं तो कहीं से उतरकर कहीं की ओर चली जाती है
मुझे रास्ते के रूप के अपने किनारे देती है।
नदी किनारे लोग फसल उगाते हैं।
ठीक ही है।
हमें नदी किनारे-किनारे चलना चाहिए,
जिन्हें मछलियां मिलती होंगी वापसी में
मिलती होंगी
जिन्हें कुल्हाड़ियां मिलती होंगी
मिलती होंगी।
उन्हें नहीं मिलती होंगी पानी की छींटे
वे एक से दूसरे शहर तक चलकर नहीं जा पाते होंगे
नदी किनारे-किनारे
उन्हें नहीं मिलते होंगे कहीं किसी अनजान तट से बहकर आए
पूजा के भीगे भटके फूल।
कविता, कहानी, निबंध लेखन में सक्रिय। भिन्न वेबसाइट और पत्रिकाओं में कविताओं और कहानियों का प्रकाशन। कविताओं और लेखों का अनुवाद भी प्रकाशित। फिल्मों और किताबों की समीक्षाएं प्रकाशित। हंस और तद्भव जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लेख और कहानियों का प्रकाशन। फिलहाल गुरुग्राम में क्वालिटी एनालिस्ट के बतौर कार्यरत और स्वतंत्र लेखन में सक्रिय।
दीप्ति पाण्डेय 
एक भ्रम ही दे दो…
लोहे को पिघलाकर भर दो
इन सपनीली आंखों में
शायद इनकी जिजीविषा वाष्प बनकर उड़ जाए
या कि कुरेदो अपने अविश्वास के नुकीले नाखूनों से
मेरी आत्मा में पड़े वयोवृद्ध घाव रिसने लगें अनवरत
और मिले उन्हें शाश्वत युवा होने का वरदान
मेरी उम्र का वह इकलौता एकाकी खाना भर दो छल से
जिससे फिर कभी किसी से आस न आए
ऐसा हो कि,
गले में अटके प्राणों की रस्साकस्सी से निकले विषाद
जीवन चाक पर कच्ची मिट्टी सा भ्रम ले आकार
और मैं कहूं कि एक सुन्दर सपना देखा विगत रात
एक भ्रम ही दे दो मुझे
कि जी पाऊं अपने शेष पलों में |
मृतक की आत्मा को शान्ति मिले
बर्फीले तूफानों में भी चूल्हे ठन्डे नहीं हुए
लकड़ियां, काठ कोठार में भरी रहीं
गडरियों की भेड़ें बनी रहीं श्रेष्ठ अनुयायी
और अपने मालिक द्वारा तय रेख पर बढ़ती रहीं अनजान राह
लेकिन मालिक जो गढ़ता रहा अपना रास्ता
बर्फीली चट्टानों के बीच बिना किसी अनुसरण के
उसकी कुल जमा आमदनी हर दिन चूल्हे को आग देना था
एक दिन काठ कोठार में रखी महीनों से प्यासी लकड़ियां
दिखती हैं भीगी, सीली-सीली
ताप और हिमांक में सांठ-गांठ देखी जाती है
गडरिए के चूल्हे को आग की जगह धुआं मिलता है
भेड़ें, बर्फीली चट्टान पर चढ़ते हुए
गीली लकड़ियां चूल्हे से धुआं उलीचते हुए थक चुकी हैं
और भूख से हारा गड़रिया
जीवन के ताप से मुक्त हो ठंडा पड़ चुका है
सभा में लोग कहते हैं – मृतक की आत्मा को शान्ति मिले
युद्ध पुत्रियां और तितलियां
मुझे क्षमा करना मेरे साथी
मैं नहीं उगा पाऊंगी उन स्त्रियों को
अपनी कविताओं के खेतों में
बथुआ और गाजर घास की तरह
जो युद्धरत भूमि में
धूल पर ख़ून गिरने से जन्मी थीं
इसलिए तुम्हारी कविता को सिरे से नकारती हूं मैं
इतिहास में दर्ज है कि –
खेतों में तितलियों के पीछे दौड़ते-दौड़ते
अनजाने युद्ध का हिस्सा बन जाने वाली गुड़ियाएं
अपनी कोख को सहलाते हुए
अपनी दादियों, माँओं की वीरता के किस्से सुनाती थीं
ओ मेरी आजाद तितलियों –
मेरी माँ आग से बनी थी
वो चूल्हे के धधकते अंगारों के बीच से
रोटी को जलने से बचा सकती थी
धूल और ख़ून से जन्मी ये युद्ध पुत्रियां
फिर जन्मती हैं – तितलियां
नहीं-नहीं, कैद तितलियां
मुझे माफ करना प्रिय,
मैं भी युद्ध से जन्मी हूं
विशेषाधिकारों और उपेक्षाओं के द्वन्द्व की ज़मीन पर
अभी मीलों लम्बी यात्रा पर जाना है मुझे
मेरा सामान मुझे ही तय करना होगा
तुम्हारी थोपी गई दया और असमानता को
अब नहीं ढो पाऊंगी मैं
मेरी कविताओं की देहरी से भीतर
आ सकते हो तुम भी बेहिचक
बांच सकते हो अपनी नई कविता – स्त्री विमर्श पर
मैं सुनना चाहती हूं एक पुरुष देह से स्त्री मन को
आना मेरे साथी
लेकिन आधे मत आना
अपने भीतर एक बटा दो स्त्री भी लाना
चित्रकार, illustrator, कवयित्री, दर्शनशास्त्र की शोधार्थी, साहित्य में विशेष अभिरुचि
रमेश प्रजापति
जीवित हैं मेरे भीतर पिता
दिनभर मज़दूरी की थकान की ऊब के बावजूद
उम्रभर पूरी नींद नहीं सो पाये पिता
उनके सपनों में साहूकार का डर सताता रहता
अचानक रात में उठते बड़बड़ाते
और बैठ जाते हुक्का गुड़गुड़ाने
पिता का शोषण साहूकार ने ही नहीं
बल्कि उनके चाहने वालों ने भी जी भर किया
उनके अनुभवों की सीढ़ी पर चढ़ते
हमेशा उन्हें नीचे खिसकाते रहे
झुकते रहे कंधे
न जाने किस उम्मीद में संबंधों के बोझ को ढोते रहे पिता
झल्लाती माँ पिता को देती रहती नसीहत
परंतु अजीब मिट्टी के बने थे पिता
अपने लिए जीने से ज़्यादा हमेशा दूसरों के लिए मरते रहे ताउम्र
और घर सिकुड़ते हुए एक गिलास पानी में समा गया
रोज़ी रोटी की तलाश में मुझे दिल्ली भेजकर
पिता ने ली राहत की सांसें
जिन्हें महसूस किया मैंने अपने भीतर
एक दिन गहरी नींद में ऐसे सोये पिता
कि उसके बाद कभी नहीं उठे
चाक उनके उठने की प्रतीक्षा में एक अड़वासी चुपचाच बैठा है
और माँ उदासी में लिपटी है
बावजूद इसके मेरे भीतर आज तक जागे रहते हैं पिता।
भूख में खनकते शब्द
अतीत की गलियों में कूदते-फांदते
धूल में लिपटे कुछ शब्द
वर्तमान के कोलाहल को तोड़कर
ध्वनित होते हैं मेरे एकांत में
छतनार पेड़ पर परिंदों के कलरव में
गूलर की मिठास से घुले हैं कुछ शब्द
मेरे भीतर उगा जीवन का पेड़
वक़्त की धूप में ठूंठ हो गया
गीली मिट्टी में सने शब्दों को लोकधुन में गुनगुनाता है चरवाहा
गोधुलि में बजती टालियों से टुनटुनाते शब्दों से
पुलकित हैं जीवन के बीहड़ रास्ते
खोरा लगी दीवारों से
धरती की परात में रात-दिन
चून-सा झरते हैं स्मृतियों के शब्द
वक़्त की सूखी नदी में
किरकिरा रहे सीपियों से कुछ शब्द
जब कुछ नहीं बचता तब भी
हमारे भीतर के कुएं में
तैरते रहते हैं आत्मीय शब्द
तुम जब सामने होती हो तब भी मौन भाषा में
लहरों से छिटके कुछ शब्द
ओस की बूंद से ठहरे तुम्हारे पपड़ाये होंठों पर
दूर तक फैली नीरवता को गुदगुदाते हैं
भादों की धूप में बाजरे के दाने से
चिड़िया के सपने में
अच्छे दिनों से चाह में
भूखे बच्चे की भूख में खनकते हैं कुछ मीठे शब्द।
आधा चांद
पूरे आसमान में
अच्छा नहीं लगता आधा चांद
माँ हो जाती है दुखी
पूरी अंधेरी रात में
तुम मत आना अधूरे मन से
हमारे बीच पसरे मौन से अवरुद्ध हो जाता है गला
माना कि आधी रोटी बहुत होती है भूख से कुनमुनाते पेट में
परंतु पूरे दिन की आधी मजदूरी से
भर नहीं पाता पूरे घर का पेट
हमारी आंखें चकाचौंध में डूबी
आधा-अधूरा ही देख पाती है सच
और हमारे कान कभी-कभी नहीं सुन पाते पूरी बात
आधा-अधूरा गीत
आधा-अधूरा मीत
आधा-अधूरा खिला फूल
आधी-अधूरी बात
आधा-अधूरा प्रेम
आधा-आधा चांद
जब भी पूरी तरह से नहीं खुलते तो उदासी से भर देते हैं
जीवन आधा कर देते हैं
भयावह अंधेरी रात से तो बेहतर होता है
अंधेरे के वर्चस्व को तोड़ता आधा चांद।
स्त्री की हंसी
यूं ही नहीं हंसती स्त्री
अनगिनत राज़ छुपे होते हैं उसकी हंसी में
मोनालिसा के होंठों में दबी
ज़रा-सी हंसी का राज
आज तक नहीं समझ पायी दुनिया
स्त्री के हंसते ही कांपने लगते हैं दमदार वृक्ष
हिलने लगती हैं सत्ता की चूलें
झुकने लगती हैं मद में अकड़ी गर्दनें
माथे पर उभरने लगती हैं सिलवटें
ख़ौफ़ के मारे छुईमुई से मुरझा जाते हैं रौबदार चेहरे
स्त्री के हंसते ही
उसके होंठों से सिर्फ खुशी के फूल ही नहीं झरते
बल्कि उदासी की पंखुड़ियां भी गिरती हैं
उसके हंसते ही
अंधकार से भरा आकाश जगमगा उठता है
धरती के आंगन में टपकने लगते हैं चांदनी के शूल
स्त्री की उन्मुक्त हंसी से
परम्पराओं की छाती में चुभते हैं सूल
आदर्शों की उड़ती हैं धज्जियां
मर्यादाओं की टूटती हैं बेड़ियां
रूढ़ियों के चटकते हैं धागे
उन्हें रुलाने ही जब हो रही हों पुरजोर कोशिशें
तब मर्दवादी मानसिकता के वर्चस्व की
तोड़ सब बंदिशें
तुम हंसो!
कि तुम्हारे हंसने से आह्लादित होता है जीवन।
कवि और लेखक रमेश चंद के अब तक चार कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें ‘पूरा हंसता चेहरा’, ‘शून्यकाल में बजता झुनझुना’ एवं ‘भीतर का देश’ प्रमुख हैं। आपकी कविताएं देश की विभिन्न भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। आपको 2015 में शिक्षक साहित्यकार सम्मान, लखनऊ से नवाज़ा जा चुका है।
हेंकर रोकोम बाडो (गालो भाषा)

बाजरा और धान के दानें
जिनके लिए जीवन तत्व हों,
खेत-खलिहान जिनका कर्म क्षेत्र हो
सुनो सदा मेरी-
वन, पेड़ और पौधों की अहमियत क्या है?
आज मैं बताऊंगा
अपने गीत से एक कहानी सुनाऊंगा।
वन, उपवन, पेड़, पौधे गर न रहे
तो वर्षा ऋतु में गगन
काले मेघ रहित हो जाएगा,
और वह धरती को जल नहीं दे पाएगा।
नदियों और झरनों के जीवन्त नहीं होने से
खेतों में रोपण नहीं हो पाएगा।
इसलिए बिन देखे, बिन सोचे पेड़ों की कटाई न करो,
वन-उपवन की रक्षा करो।
‘हिरी’, ‘हिलोक’, ‘कोबो’ और ‘कोआक’ प्रजाति के बड़े-बड़े पेड़
जिन्हें हम रोज़ देखा करते थे
धनवान और बलवान के गृह निर्माण में लुप्त हो गए,
जंगल को सजाती बांसों की प्रजातियां
और जल प्राणियों से भरी नदियां
बद्धिजीवियों के भोग-विलास के हत्थे चढ़ गए।
है कोई यहां एक धरती पुत्र
जो इन बातों के ख़िलाफ़ आवाज बुलंद करेगा
और इन प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण की मुहिम उठाएगा?
—
सियांग तुम माँ हो,
माँ ही बनी रहना।
तुम्हारे किनारों से बसे जन समुदायों में
तुम्हारे नाम से जरित लोगों में
प्यार सदा पलता रहे,
एकता सदा बनी रहे।
यह जो धरती का परिदृश्य है
कभी बदलने वाला नहीं,
ये पहाड़ ये नदियां
अपनी जगह त्यागने वाले नहीं।
पूरब और पश्चिम कहकर
जिलों का नामांकरण इंसानों ने किया,
ईश्वर का इसमें हाथ नहीं।
बोलियों में ज़रा सा अन्तर
दिलों में दूरी का कारण न बने
दोस्त-दोस्त को प्यार करते रहें
सगे-संबंधियों का बन्धन बना रहे।
किसी तुच्छ कारण से
कड़वाहट से भरे चन्द लोग
कुछ कड़वे शब्द बोल भी दें,
संकीर्ण सोच वाले चन्द लोग
इधर की बात उधर कह भी दें,
समाज के सुजनों से सुमति बनी रहे,
बड़े-बुजुर्गों के आपसी वार्तालाप से
समस्याओं का हल होता रहे
और समाज को बिखरने न दे।
—
नए ज़माने की पढ़ी-लिखी
गालो समाज की युवतियो!
नए दौर की जागरूक
गालो की समाज महिलाओ!
राह में पड़ा वृक्ष न बनो
कि लोग ऊपर से गुजर जाएं।
सूखे पत्तों सी कमजोर न बनो
कि बेकार समझकर लोग उपेक्षा करें।
बुद्धि और विवेक के सहारे
सफल और सशक्त जीवन जियो।
प्यार से संजोयें घर आंगन
जहां गहरे रिश्तों की नींव हो,
किसी की नासमझी और बे-मुरव्वती के कारण
एक नारी दूसरे का हक़ न छीनने पाये,
एक दूसरे को ख़ून के आंसू न रुलाए।
माँ-बाप जब उम्र के आख़िरी पड़ाव में होंगे,
उम्र की ढलान में जब उनके तन निर्बल हो जाएंगे,
और वे घर की सम्पति अपने बच्चों में बांटेंगे,
तब केवल बेटों को न देकर
बेटियों को भी हिस्सेदार बनाएं,
यह पैगाम समाज तक पहुंचाओ
आज की सबल गालो नारी हो तुम।
हेंकर रोकोम बाडो गालो भाषा के कवि हैं, मुख्य अभियन्ता पद पर कार्यरत हैं, गालो भाषा में गीत और कविताएं रचते हैं।

